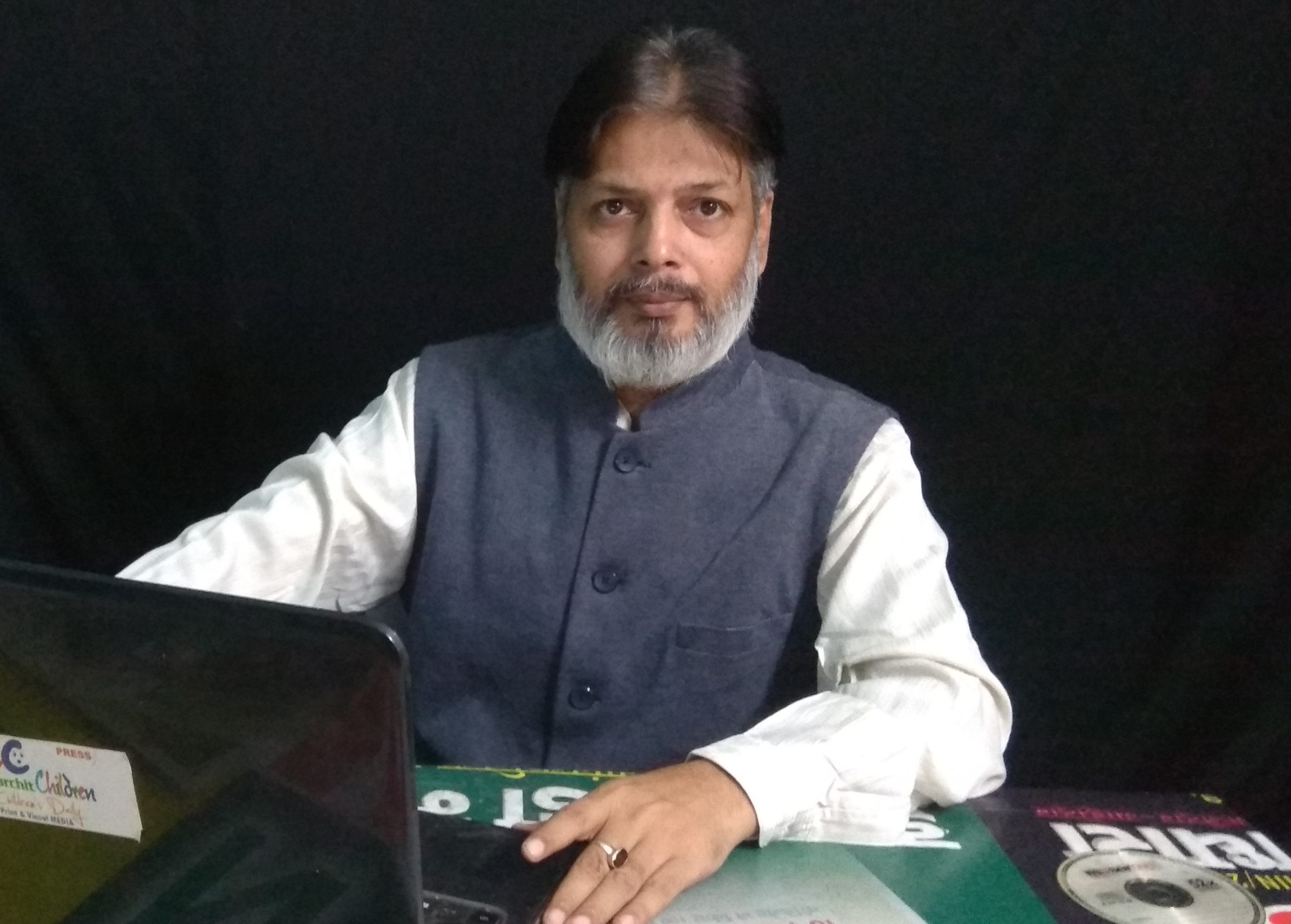सम्पादकीय : पूर्णेन्दु सिन्हा ‘पुष्पेश ‘
युद्ध का दौर है दोस्तो। गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, दुश्मन के इलाके में हमारे जवान घुसकर जवाब दे रहे हैं। ऐसे माहौल में हर किसी की नजर एक तरफ है – बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ – टीवी, मोबाइल और न्यूज़ चैनलों पर। सबको यह जानना है कि अब क्या हुआ? कौन जीता? किसने जवाब दिया? और ऐसे वक्त में मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? यही बात आज सबसे जरूरी है समझने की।
हम सब जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यानी संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद मीडिया ही वो ताकत है जो जनता की आवाज बनती है। पर जब देश पर हमला हो, जब जंग छिड़ जाए, तब क्या मीडिया को उसी तरह काम करना चाहिए जैसे आम दिनों में करता है? क्या युद्धकाल में भी प्रेस की आज़ादी उतनी ही खुली होनी चाहिए? या कुछ सीमाएं तय होनी चाहिए? ये सवाल आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने कुछ डिजिटल मीडिया संस्थानों पर पाबंदी लगाई है। द वायर का उदाहरण सबके सामने है, जिनके प्रसारण पर रोक लगी है और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। इसे लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेस की आज़ादी पर हमला है। पर क्या वाकई ऐसा है? या वाकई राष्ट्रहित पहले है? चलिए इस पर ठंडे दिमाग से बात करते हैं।
सबसे पहले बात यह समझें कि युद्ध अब केवल मैदान में लड़ी जाने वाली चीज नहीं रह गई। ये लड़ाई अब इंटरनेट, न्यूज़, सोशल मीडिया और दिमाग में भी लड़ी जाती है। इसे हम ‘सूचना युद्ध’ (information warfare) कहते हैं। यानी अगर दुश्मन को पता चल जाए कि हमारी सेना कहां तैनात है, किस इलाके में कितने जवान हैं, कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है — तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगें जो हमारे देश के मनोबल को गिरा दें, या जनता में अफरा-तफरी फैला दें, तो वह भी नुकसानदेह है।
अब ऐसे में सरकार के पास कुछ अधिकार होते हैं; जैसे IT एक्ट की धारा 69A। इसके तहत सरकार उन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स या न्यूज़ पोर्टल्स पर रोक लगा सकती है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हों। और युद्धकाल तो वैसे भी असाधारण समय है।
तो सवाल ये नहीं है कि प्रेस की आज़ादी खत्म हो रही है। असल सवाल ये है कि क्या पत्रकारिता भी उतनी ही जिम्मेदारी निभा रही है जितनी इस समय जरूरी है? पत्रकारों को यह समझना होगा कि हर खबर ब्रेक करने की होड़ में कहीं वो अनजाने में दुश्मन की मदद तो नहीं कर रहे? सेना की गोपनीय बातें या ऑपरेशन की जानकारी लीक कर रहे हैं क्या? या फिर ऐसी खबरें फैला रहे हैं जिससे आम जनता का हौसला टूटे?
मीडिया को यह भी सोचना होगा कि युद्ध के वक्त देश में डर, बेचैनी और अफवाहें पहले से ही बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर मीडिया दिनभर हताहतों की खबरें, हार-जीत की अधूरी बातें, या बिना जांचे-परखे खबरें फैलाएगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मीडिया की असली ताकत इस समय ये है कि वो सच्ची, संतुलित, और भरोसेमंद खबरें दे ताकि लोगों का मनोबल बना रहे, समाज में एकता बनी रहे, और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे।
दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों में युद्धकाल में मीडिया पर सख्त नियंत्रण रहता है। वहां मीडिया अपनी सेना के मिशन या ऑपरेशन की जानकारी तब तक नहीं दिखाता जब तक सेना इजाजत न दे। भारत में भी 1971, कारगिल युद्ध के समय हमने देखा कि जब मीडिया ने राष्ट्रवादी भावना के साथ खबरें दिखाई, तब देशभर में एकजुटता की लहर आई।
आज का जमाना डिजिटल है, सोशल मीडिया का दौर है। दुश्मन देश तो अफवाहें फैलाने के लिए बैठा ही है। वह फर्जी तस्वीरें, झूठी खबरें और झूठे आंकड़े फैलाकर भारत की जनता को भ्रमित कर सकता है। इसलिए मीडिया का फर्ज है कि वह फेक न्यूज की पहचान करे, उसका खंडन करे और जनता को सही बात बताए।
युद्धकालीन पत्रकारिता का मकसद सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं है। ये समय है शांति का संदेश फैलाने का, सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने का, और समाज को जोड़कर रखने का। हमें याद रखना चाहिए कि पत्रकारिता कोई सरकारी प्रचार तंत्र नहीं है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सेना के ऑपरेशन का सीधा-सीधा लाइव टेलीकास्ट कर दें। हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है।
मीडिया को सेना और सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलना चाहिए। सेना जो दिशा-निर्देश देती है उसका पालन करना चाहिए। इस समय हमें आलोचना या बहस से ज्यादा देश की सुरक्षा और अखंडता की चिंता करनी चाहिए। आलोचना करने का समय भी आएगा, अभी देश के साथ खड़े रहने का वक्त है।
इतिहास भी यही बताता है। 1962 में चीन से युद्ध के वक्त जब मीडिया को पूरी जानकारी नहीं थी और जनता को भ्रमित कर दिया गया, तब नुकसान हुआ। लेकिन 1971 और कारगिल युद्ध के वक्त मीडिया की जिम्मेदारी और राष्ट्रहित वाली पत्रकारिता ने जनता को भरोसा दिया।
अभी भी वक्त है कि हम अपनी पत्रकारिता की दिशा तय करें। मीडिया हाउस को अपने रिपोर्टरों को युद्धकाल की ट्रेनिंग देनी चाहिए – कैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करें, कैसे सुरक्षा का ध्यान रखें, और कैसे सेना की गोपनीयता बनी रहे। साथ ही एक आचार-संहिता (code of conduct) भी बननी चाहिए ताकि पत्रकार जाने-अनजाने में गलतियां न करें।
अंत में कहने का मतलब यह है दोस्तो – प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र की जान है, लेकिन युद्धकाल में राष्ट्र की रक्षा, जनता का मनोबल और देश की छवि सबसे ऊपर है। मीडिया को समझना होगा कि आज उनकी कलम सिर्फ खबर नहीं लिख रही, वह देश के भविष्य की कहानी लिख रही है। इसलिए ज़िम्मेदारी से लिखें, देशहित में लिखें और ऐसा लिखें कि जब युद्ध खत्म हो तो हम गर्व से कह सकें – “हमारे मीडिया ने भी देश की रक्षा में अपना फर्ज निभाया था।”
जय हिंद!!